Marxist theory of rights
Hello दोस्तों ज्ञानउदय में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बात करते हैं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में । इस Post में हम जानेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत के उदय, उसका अर्थ और विशेषताओं के बारे में, तो चलिए जानते हैं आसान भाषा में ।
मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय
जैसे उदारवाद का उदय सामंतवादी व्यवस्था के अवशेषों पर हुआ है, वैसे ही मार्क्सवाद का उदय पूंजीवादी वर्गविभाजित समाज की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरुप हुआ है । जहां पर उदारवाद ने सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ स्वतंत्रता का नारा बुलंद किया है । उसी तरह से मार्क्सवाद का मूल मंत्र वर्ग विभाजित समाज को बदलकर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना माना जाता है ।
राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को पढ़ने के लिए यहाँ Click करें |
मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी राज्य में, किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग (डोमिनेंट क्लास) के अधिकार होते हैं । अतः कामगार वर्ग की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वह पूंजीपति वर्ग को शासन से हटाकर स्वयं सत्ता प्राप्त कर ले । चुकी अधिकार सदैव राज्य के वर्ग चरित्र से जुड़े रहते हैं, इसलिए पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अधिकारों का स्वरूप अलग-अलग होता है ।
पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के अधिकारों का स्वरूप
पूंजीवादी व्यवस्था का उदय औद्योगिक क्रांति के पश्चात मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था की मांग के फल स्वरुप हुआ है । यह व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित है । इसमें स्वतंत्रता और समानता को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है, जहां तक वह मुक्त प्रति स्पर्धा को बढ़ावा देते हैं । साथ ही साथ इसमें संपत्ति के अधिकार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है । इसमें निजी संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर पूंजीपति वर्ग, प्रभुत्व शैली वर्ग की भूमिका संभाल लेता है तथा कामगार वर्ग की स्थिति पराधीन वर्ग की हो जाती है ।
उल्लेखनीय है कि मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में पूंजीवादी राज्यों द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों के असलियत का विश्लेषण किया है और इस व्यवस्था के अंतर्गत मजदूर वर्ग को दिए गए अधिकारों को बिल्कुल खोखला बताया है । उसने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में कानून की दृष्टि से सभी नागरिकों के समान अधिकार स्वीकार किए जाते हैं, परंतु वास्तविक स्तर पर सभी अधिकार पूंजीपति वर्ग के अधिकार होते हैं । कामगार वर्ग के अधिकार कभी भी वास्तविक नहीं हो पाए ।
समाजवादी व्यवस्था में अधिकारों का स्वरूप
मार्क्सवाद के अंतर्गत समाजवादी स्थिति वह व्यवस्था है, जब कामगार वर्ग पूंजीपतियों को हटाकर उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित कर देता है । सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद राज्य लुप्त हो जाता है तथा एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है । पहली अवस्था को समाजवाद कहा जाता है । इसमें समाज के संसाधनों पर सर्वहारा वर्ग का स्वामित्व स्थापित हो जाता है, हालांकि इस अवस्था में वर्ग विभाजन बना रहता है तथा इसके आगे की दूसरी अवस्था साम्यवाद की अवस्था आ जाती है । जब साम्यवाद की स्थापना हो जाती है, तब राज्य तथा वर्ग दोनों ही विलुप्त हो जाते हैं तथा एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाती है ।
संपत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को पढ़ने के लिए यहाँ Click करें |
इन दोनों अवस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियां पूरी तरह विकसित नहीं होती । अतः सभी कामगारों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होता । परंतु साम्यवाद के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं और सब कामगारों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो जाता है ।
यह तो स्पष्ट है कि समाजवाद के अंतर्गत कामगार वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग होता है । अतः इनको वास्तविक अधिकार प्राप्त होते हैं । परंतु उत्पादन की शक्तियों के पूरी तरह विकसित ना होने के कारण कामगार वर्ग के अधिकार अब भी पूंजीवादी ढंग से ही निर्धारित होते हैं । अर्थात
“हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपने कार्य के अनुसार। “
परंतु साम्यवाद के अंतर्गत जब उत्पादन की शक्तियां पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तो कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है । तब एक नई अधिकार व्यवस्था लागू हो जाती है । इसे इस सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है कि
“हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार तथा हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार ।”
साम्यवादी देशों में दिए गए अधिकारों की वास्तविकता
यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है की मार्क्सवादी चिंतन की प्रेरणा के फल स्वरुप रूस में 1917 की क्रांति के पश्चात साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई तथा उसमें नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी विचार किया गया था । लेकिन 1936 में रूस में स्टालिन संविधान में मौलिक अधिकारों का एक अध्याय शामिल किया गया । सोवियत संघ के 1977 के संविधान द्वारा आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया । सोवियत नागरिकों को रोजगार के अवसर के साथ-साथ अपनी पसंद के व्यवसाय चुनने का अधिकार, विश्राम, अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा जैसे विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए । साथ ही वाणी, विचार, अभिव्यक्ति, प्रकाशन एकत्र होने तथा सभा या जुलूस करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई ।
कार्ल मार्क्स एक समाजवादी वैज्ञानिक के रूप में पढ़ने के लिए यहाँ Click करें |
लेकिन इन अधिकारों पर एक प्रतिबंधित था, वह यह की इन अधिकारों का प्रयोग जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही किया जा सकता था । इसके साथ एक सच्चाई और यह भी है कि समाजवादी देशों में जनसाधारण के हितों को परिभाषित करने का अधिकार, साम्यवादी दल के उच्च अधिकारियों को ही प्राप्त था । इसी वजह से आम नागरिक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुलकर प्रयोग नहीं कर सकते थे ।
इस तरह से 1981 में ‘ग्लासनोस्त’ की नीति के द्वारा अधिकार व्यवस्था को अपेक्षाकृत उदार बनाने का प्रयत्न किया गया । परंतु देश की बिगड़ती हालात में 1991 तक वहां समाजवादी व्यवस्था को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया था । इसी तरह से चीन के संविधान में भी मौलिक अधिकारों की एक लंबी सूची दी गई है । इसमें किसी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करने का अधिकार, भाषण, संघ बनाने, जुलूस प्रदर्शन का अधिकार भी प्रदान किया गया है तथा इन पर कोई संवैधानिक और कानूनी बंधन नहीं लगाए गए हैं ।
इसी तरह से अनेक सामाजिक और आर्थिक अधिकार जैसे काम, रोजगार, आराम, शिक्षा तथा पेंशन भी दिए गए हैं । परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है । यह चारों तरफ से राज्य द्वारा आरोपित कठोर बंधनों से गिरे हुए हैं । जो व्यक्ति राज्य की गतिविधि से अलग विचार रखते हैं, उन्हें देशद्रोही या क्रांति विरोधी कहकर बड़ी आसानी से दबाया जा सकता है ।
निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो साम्यवादी देशों में दिए जाने वाले अधिकार वास्तविक नहीं है । अतः यह आरोप उदारवादी लेखक आरंभ से लगाते रहे हैं और ऐसे ही आरोप साम्यवादी भी उदारवादियों पर लगाते रहे हैं । यह सत्य है कि जीवन की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को दोनों ही व्यवस्थाओं में पूरा कर लिया गया है । जरूरत तो है कि साम्यवादी व्यवस्था में लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार किए जाएं । इसके अंतर्गत मुख्यत दूसरे दलों का निर्माण, विचारों की स्वतंत्रता,विपक्षी दलों को मान्यता, प्रेस तथा संगठनों को पार्टी नियंत्रण से मुक्ति तथा पार्टी में लोकमत को बढ़ावा दिया जाए, ताकि नागरिकों के अधिकार वास्तविक की कसौटी पर खरे उतर सकें ।
तो दोस्तों इस Post में हमने जाना अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में । अगर आपको यह Post अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर Share करें । तब तक के लिए धन्यवाद !!


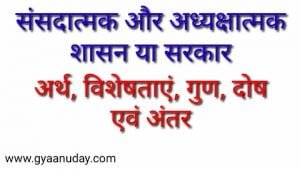
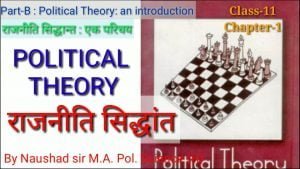
Pingback: संस्कृतिकरण क्या है – Gyaan Uday